(नवं सर्ग में से) ;
दो वंशो में प्रकट करके पावनी लोक - लीला ,
सौ पुत्रो से अधिक जिनकी पुत्रिया पूत्शीला ,
त्यागी भी है शरण जिनके , जो अनाशक्त गेही ,
राजा - योगी जय जनक वे पुन्यदेही , विदेही |
विफल जीवन व्यर्थ बहा , बहा ,
शरद दो पद भी न हुए हाहा!
कठिन है कविते, तुम भूमि ही ,
पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा |
करुणे , क्यों रोती है ? 'उत्तर ' में और अधिक तू रोई ,
'मेरी विभूति है जो, उसके भव - भूति क्यों कहे कोई' !
अक्साध को अपनाकर त्याग से,
वन तपोवन सा प्रभु ने किया |
भरत ने उनके अनुराग से,
भवन में वन का व्रत ले लिया |
स्वामी सहित सीता ने
नंदन मन सघन - गहन कानन भी,
वन उर्मिला वधु ने
किया उन्ही के हितार्थ निज उपवन भी !
अपने अतुलित कुल में
प्रकट हुआ था कलंक जो कला ,
वह उस कुल - बाला में
अश्रु - सलिल से समस्त धो डाला|
भूल अवधी - सुध प्रिय से ,
कही जगती हुई कभी - 'आओ! '
किन्तु कभी सोती तो
उठती वह चौंक बोलकर - 'जाओ! '
मानस मंदिर में सटी , पति की प्रतिमा थाप ,
जलती - सी उस विरह में , बनी आरती आप!
आँखों में प्रिय - मूर्ति थी , भूले थे सब भोग;
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग !
भवन में वन का व्रत ले लिया |
स्वामी सहित सीता ने
नंदन मन सघन - गहन कानन भी,
वन उर्मिला वधु ने
किया उन्ही के हितार्थ निज उपवन भी !
अपने अतुलित कुल में
प्रकट हुआ था कलंक जो कला ,
वह उस कुल - बाला में
अश्रु - सलिल से समस्त धो डाला|
भूल अवधी - सुध प्रिय से ,
कही जगती हुई कभी - 'आओ! '
किन्तु कभी सोती तो
उठती वह चौंक बोलकर - 'जाओ! '
मानस मंदिर में सटी , पति की प्रतिमा थाप ,
जलती - सी उस विरह में , बनी आरती आप!
आँखों में प्रिय - मूर्ति थी , भूले थे सब भोग;
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग !
आठ पहर चौंसठ घड़ी स्वामी का ही धयान,
छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान !
उस रुदंती विरहणी के रूदन - रस के लेप से'
और पाकर ताप उसके प्रिय - विरह विक्षेप से ,
वर्ण - वर्ण सदैव जिनके हो विभुसन कर्ण के ,
क्यूँ न बनते कवी जानो के ताम्रपत्र सुवर्ण के ?
पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्नाप्रिया आब थे ,
छीटें वहीँ उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे आब थे?
उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट,
धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओंट|
मिलाप था दूर अभी धनी का,
विलाप ही था बस का बनी का |
अपूर्व आलाप वाही हमारा ,
यथा विपंची - दिर दार दारा|
सींचे ही बस मालिनें, कलश लें,कोई न ले कर्त्तरी ,
शाखी फूल फले यथेच्छ बढ़के ,फैले लताएं हरी|
क्रीडा कानन शैल यन्त्र-जल से संसिक्त होता रहे,
मेरे जीवन का,चलो सखी,वही सोता भिगोता बहे!
क्या क्या होगा साथ,में क्या बताऊँ!
है ही क्या,हाँ! आज में जताऊं?
तो भी तुली पुस्तिका और वीणा,
चथ्वी में हूँ,पांचवी तू प्रवीणा!
हुआ एक दुःख स्वप्ना सा,कैसा उत्पात,
जागने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात!
खान पान तो ठीक है पर तदन्तर हाय!
आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय?
आरी व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई ,
हटा थल,तू तू क्यूँ इसे आप लायी?
वही पाक है,जो बिना भूख भावे,
बता किन्तु तू ही,उसे कौन खावे?
हे तात ,तालसंपूतक तनिक ले लेना ,
बहनों ,को वन उपहार मुझे है देना|
"जो आज्ञा,"- लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में,
ज्यों घुसे सूर्य-कर-निकर सरोज - पुटी में|
जाकर परन्तु जो उन्होंने देखा,
तो दिख पड़ी कोणस्थ वहां उर्मिला - रेखा|
यह काया है या शेष उसीकी छाया,
छन भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया|
मेरे उपवन के हरिन , आज वनचारी,
में बाँध न लुंगी तुम्हे,तजो भय भरी|
गिर पड़े दौड़ सौमित्री प्रिय पद तरा में ,
वह भींग उठी प्रिय चरण धरे दृग-जल में|


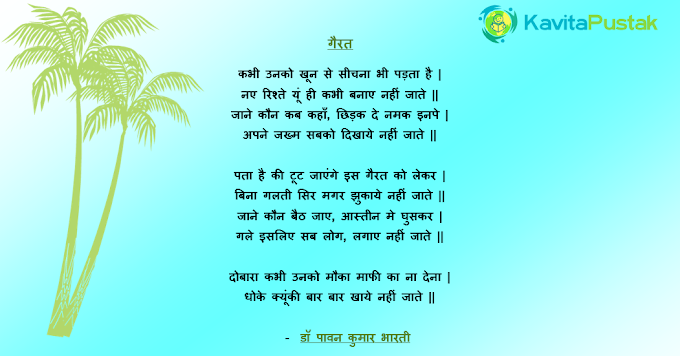

0 Comments